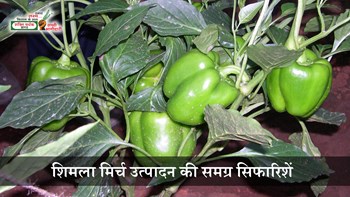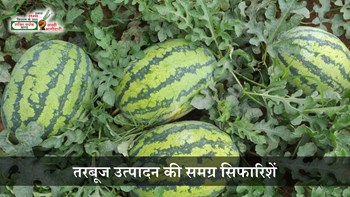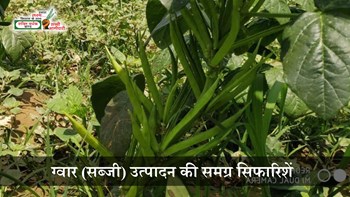कृषि जलवायु परिस्थितियां: बेल वाली फसल के फल वहां बढ़िया ढंग से पनपते है जहां गर्म-सुखा मौसम हो तथा अच्छी धूप निकलती हो। ज्यादातर बेल वाली फसल के बीज तब अंकुरित होते है, जब दिन का तापमान 25°C के आसपास हो, सामान्य वृद्धि के लिए वे अनुकूल औसत मासिक तापमान के 25°C से 30°C तक की अपेक्षा करते है, तापमान 30°C से अधिक होने पर नरपुष्प की संख्या बढ़ती है, जिससे मादा पुष्प की संख्या में कमी आती है।
बुवाई की अवधि
खरीफ : जून-जुलाई
बीज दर (किलो/हेक्टेयर):
|
फसल |
बीज दर |
|
लौकी |
2.5-3.0 |
|
तौरी |
1.25-1.5 |
|
टिण्डा |
3.5-5.0 |
ग्रीष्म: जनवरी-फरवरी
|
फसल |
बीज दर |
|
करेला |
1.75-2.0 |
|
खीरा |
1.0-1.25 |
|
पेठा |
3.0-4.0 |
अंतर (सें. मी):
|
फसल |
पंक्ति से पंक्ति |
पौधे से पौधा |
|
लौकी, तौरी, करेला |
170 |
60 |
|
टिण्डा |
150 |
60 |
|
खीरा |
130 |
50 |
|
पेठा |
250 |
60 |
खाद की निर्धारित मात्रा :
खेत तैयार करते समय अच्छी तरह से विघटित एफवाईएम की 15-20 टन मात्रा का इस्तेमान करें। एन. पी.के (कि.ग्रा./हेक्टेयर) का इस्तेमाल नीचे दिए गये अनुसार चार हिस्सों में बांटकर किया जाना चाहिए :-
|
अवस्था |
एन |
के |
पी |
|
खेत तैयार करते समय |
40 |
100 |
100 |
|
बुआई के 20 दिन बाद |
40 |
0 |
0 |
|
पुष्पण से पहले |
40 |
0 |
0 |
|
पहली तुड़ाई के बाद |
40 |
0 |
0 |
|
कुल |
160 |
100 |
100 |
नोट : 40 कि.ग्रा. नाइट्रोजन = 87 कि.ग्रा. यूरिया, 100 कि.ग्रा. फास्फोरस = 217 कि.ग्रा. डी.ए.पी., 100 कि.ग्रा. पोटाश = 166 कि.ग्रा.एम.ओ.पी.
पौध सुरक्षा - प्रमुख कीट
माहो/तेला : फोरेट (थाईमेट) का 12.5 किलो/हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल, करीब 21 दिनों के लिए फसल को अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। एण्डोसल्फान (थियोडॉन) या ऑक्सी डेमेट्रॉन मिथाइल (मेटासाइस्टॉक्स) का छिड़काव 2 मिली/लीटर की दर से 10-15 दिनों के अंतराल से करे।
कुटली (माईट) / चुरदा: सल्फर 20-25 किलो/हेक्टेयर की दर से बिखराएं या डायकोफॉल (केलथेन) / डायनोकैब (काराथेन) का 1.5-2.0 मिली/लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
फल की मक्खी :
* संक्रमित फलों तथा सूखी पत्तियों को एकत्रित करके गहरे गड्डों में जला दें।
* फलों को पौधों पर ज्यादा पकने नहीं देना चाहिए।
* बेलों को नीचे से निरन्तर निराई या जुताई करने से प्युपा को बाहर निकलने में मदद मिलती है।
* फसल पर मैलाथियॉन का 2 मि.ली. या कार्बारिल या लेबायसिड का 1.25 मि.ली. या एकालक्स का 2 मि.ली. /लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
प्रमुख रोग :
रामिल फंफूद (डाऊनी मिल्डयू): मेटालेक्सिल +मैंकोजेब (रिडोमिल) का 1.5-2.0 ग्राम/लीटर की दर से छिड़काव करें। 21 दिनों से शुरु करके 15 दिन के अंदर से 2-3 छिडकाव करने पर अच्छी रोकथाम होती है।
भस्मी फफूंद (पाऊडरी मिल्डयु): सल्फर को 20-25 किलो/हेक्टेयर की दर से बिखेरे। बिखेरने का काम सुबह या शाम के दौरान करना चाहिए। गर्म धूप में बिखेरने से पौध के लिए हानिकारक हो सकता है।
फुझारियम मुरझान : फसल को बदल-बदल कर बोएं (3 साल के क्रम में)
वायरल जटिलता: वायरस वाहक तत्वों की रोकथाम करें।
नोटः उपरोक्त दी गई सभी जानकारियां हमारे अनुसंधान केन्द्रों के निष्कर्षो पर आधारित है। फसल के परिणाम मिट्टी, प्रतिकूल जलवायु, मौसम, अपर्याप्त / घटिया फसल प्रबंधन, रोग एवं कीट के आक्रमण के कारण फसल तथा पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फसल प्रबंधन हमारे नियंत्रण से बाहर है। अतः पैदावार के लिए किसान पूरी तरह जिम्मेदार है। स्थानीय कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई सिफारिशें अपनाई जा सकती हैं।